जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट - वस्त्र मंत्रालय का मंत्र
भारत में वस्त्र उद्योग एक विशाल कच्चे माल के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े कच्चे माल के आधार और सभी महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में विनिर्माण शक्ति के साथ दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र में से एक है। भारत के वस्त्र उद्योग की यह शक्ति हाथ से बुने हुए क्षेत्र के साथ-साथ मिल क्षेत्र में भी है। हैंडलूम, हस्तशिल्प और लघु स्तरीय बिजली करघा जैसे परंपरागत क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। यह उद्योग मौद्रिक रूप में औद्योगिक उत्पादन का 7 प्रतिशत, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत और देश के निर्यात से होने वाली आय में 15 प्रतिशत का योगदान करता है।
" आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया, विकास के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों को सही दिशा देने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की मांग करती है। इस तक पहुंचने के लिए, वस्त्र मंत्रालय एक अनुकूल नीति और वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है, इस उद्योग के संस्करणों को सक्षम बनाने में सुविधा प्रदान करना और निजी उद्यमियों को अपनी विभिन्न नीति पहलों और योजनाओं के माध्यम से इकाइयों की स्थापना करने में मदद कर रहा है। "
स्मृति जुबिन इरानी
केंद्रीय वस्त्र मंत्री
"मंत्रालय ने भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाने और श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है।"
अजय टमटा
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री
रेशम उद्धोग
रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना: आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2017-18 से लेकर 2019-20 तक, तीन साल के लिेए, केंद्रीय क्षेत्र योजना "रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना के चार घटक हैं:
- अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और आईटी पहल।
- बीज संगठनों और किसानों के विस्तार केंद्र
- बीज, कच्चा धागा और रेशम उत्पादों के लिए समन्वय और बाजार का विकास और
- गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस) का निर्माण, दूसरों के बीच रेशम परीक्षण सुविधाएं, कृषि आधारित और पोस्ट-कूकून प्रौद्योगिकी का उन्नयन और निर्यात ब्रांडों का प्रचार।
रेशम की कहानी कूकून से शुरू होती है
इस योजना के लिए आवंटित 2161.68 करोड़ रुपये की राशि के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि 2016-17 के दौरान 30348 मीट्रिक टन हुए रेशम के उत्पादन को स्तर से 2019-20 के अंत तक 38500 मीट्रिक टन पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए उपाय निम्नलिखित है:
• आयात के विकल्प के रूप में 2020 तक प्रति वर्ष 8500 मीट्रिक टन बिवोल्टिन रेशम का उत्पादन।
• 2019-20 के अंत तक रेशम की खेती के उत्पादकता में सुधार कर उसे प्रति हेक्टेयर 100 किग्रा से बढ़ाकर 111 किलोग्राम करने के लिए अनुसंधान और विकास।
• मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बाजार की मांग को पूरा करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करने के लिए उन्नत रीलिंग मशीनों का बड़े पैमाने पर विकास (शहतूत के लिए स्वत: रीलिंग मशीन, उन्नत रीलिंग और कताई मशीनें और वान्या रेशम के लिए बनियाड रीलिंग मशीन)
इस योजना से महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना 2020 तक, 85 लाख उत्पादक रोजगार को बढ़ाकर उसे 1 करोड़ करने में मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक रेशम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसको प्राप्त करने के लिए, भारत में 2022 तक उच्च श्रेणी के रेशम का उत्पादन वर्तमान समय के 11,326 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर 20,650 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जिससे कि इसका आयात शुन्य पर पहुंच जाएगा। शहतूत के द्वारा 4 ए ग्रेड के सिल्क के उत्पादन को 2020 तक 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। रेशमविज्ञानियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, इस योजना के कार्यान्वयन की रणनीति स्पष्ट रूप से राज्य स्तर के समन्वय पर आधारित है जिसमें अन्य मंत्रालयों की योजनाएं जैसे ग्रामीण विकास की मनरेगा, कृषि मंत्रालय की आरकेवीवाई और पीएमकेएसवाई भी शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के सहयोग से रोग प्रतिरोधी रेशमकीट, मेज़बान संयंत्र मे सुधार, उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण तथा रिलिंग और वेविंग करने वाले संयंत्रों के लिए अनुसंधान और विकास की योजना को पूरा किया जाएगा।
रेशम के कीड़ों के लार्वा की नई किस्म:
केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) ने कूकून की उत्पादकता को बढ़ाने और सेरीकल्चर में लगे हुए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए शहतूत और वान्या के रेशम कीटों के नव-विकसित प्रजातियों को अधिसूचित किया है। कूकून की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कृषि-जलवायु के लिए उपयुक्त रेशम के कीडों की नस्लें आवश्यक हैं।
ट्रॉपिकल तसर प्रजाति वाले रेशमकीट (बीडीआर-10) की उत्पादकता पारंपरिक डाबा नस्ल की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। किसान प्रत्येक 100 रोग मुक्त परत (डीएफएल) से 52 किलोग्राम तक कूकून प्राप्त कर सकते हैं। रेशम के कीड़े की इस नस्ल से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के आदिवासी किसानों को सहायता मिलेगी।
रेशमकीट की प्रजाति, मल्टीवोल्टाइन एक्स बीवोल्टाइन शहतूत हाइब्रिड (PM x FC2) से प्रति 100 डीएफएल में 60 किग्रा तक का उत्पादन हो सकता है और यह प्रजाति पहले की प्रजाति PM x CSR से बेहतर है। उच्च गुणवत्ता के रेशम और सार्थक अंडों की प्राप्ति के कारण, यह प्रजाति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों के लिए उपयुक्त है।
एरी रेशमकीट (C2) की प्रजाति 100 डीएफएल में 247 की संख्या में एरी कूकून का उत्पादन कर सकती है। यह प्रजाति, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए उपयुक्त है।
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाला केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशमकीट के बीजों की नई प्रजातियों के विकास के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगा हुआ है और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक उपयोग करने से पहले व्यापक क्षेत्र परीक्षण करता है।
समन्वित सिल्क विकास योजना (आईएसडीएस):
"कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए सामर्थ योजना: केंद्रीय वस्त्र मंत्री, स्मृती ज़ुबिन इरानी ने मई, 2018 को नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आनेवाले सामर्थ योजना- कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, के बारे में बताने और इसके दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस नई योजना का व्यापक उद्देश्य, कताई और बुनाई को छोड़कर, कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर युवाओं को पकड़ बनाने के लिए उन्हें लाभकारी और स्थायी रोजगार के लिए निपुणता प्रदान करना है।
इस बैठक में पिछली योजना के कार्यान्वयन के समय हितधारकों की चिंताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। संबंधित हितधारकों से इस बात पर भी फीडबैक लिया गया कि यह योजना वस्त्र उद्योग में किस प्रकार से योगदान दे सकती है और उसे लाभान्वित कर सकती है तथा कौशल विकास को बढ़ावा दे सकती है।
योजना के दिशा-निर्देशों को 23 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। इस योजना का अनुमोदन 20 दिसंबर 2017 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 1300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किया गया। इसका उद्देश्य मांग की पूर्ति करने, कपड़ा उद्योग में रोजगार सृजन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उसे पूरक बनाने के लिए प्लेसमेंट-उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) कौशल कार्यक्रमों का अनुपालन करना है। इस योजना का लक्ष्य 3 वर्ष (2017-20) की अवधि में 10 लाख लोगों (संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
वस्त्र मंत्रालय में समग्र कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में पायलट योजना के रूप में 272 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया, जिसका भौतिक लक्ष्य 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना था और इसके सरकार का योगदान 229 करोड़ रूपया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य चरण में इस योजना को 1,900 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आगे बढ़ाया गया और जिसका लक्ष्य 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना था।
समग्र कौशल विकास योजना कपड़ा उद्योग में उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल श्रमशक्ति के महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है। इसे तीन घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जिसमें मुख्य जोर पीपीपी प्रणाली पर दिया गया है जहां पर मांग-पूर्ति कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने उद्योग के साथ साझेदारी विकसित की जा रही है। इस योजना को बड़े पैमाने पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के साथ जोड़ा गया है।
कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास
इस योजना के अंतर्गत कुल 11,14,545 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, मुख्य रूप अपेरल और गारमेंटिंग मे 86 प्रतिशत के साथ जिस पर 935.17 करोड़ रुपये का कुल खर्च आया। प्रशिक्षण प्राप्त 8,43,082 लोगों (75.64 प्रतिशत) को कपड़ा क्षेत्र में रोजगार दिया गया।
पिछले 4 वर्षों में प्रशिक्षित किए गए लोगों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं, जबकि 22.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और 7.22 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग थे।
कौशलता के माध्यम से अंतर उत्पन्न करना:
कपड़ा क्षेत्र में 45 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं।
वर्ष 2022 तक, लगभग 17 मिलियन अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता।
पिछले चार वर्षों में 8.58 लाख लोगों को 58 सरकारों और उद्योग भागीदारों की साझेदारी से प्रशिक्षण दिया गया।
सामर्थ दिशानिर्देशों को 23.04.2018 को जारी किया गया और इसको पूरा करने के लिए साझेदारों के मनोनयन के लिए 21.05.2018 को आरएफपी मंगाई गई।
हथकरघा क्षेत्र
एक बुनकर अपने करघे पर काम करती हुई
ब्लॉक स्तर समूह (बीएलसी)
ब्लॉक स्तर समूह (बीएलसी), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)/ कम्प्रीहेन्सिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम (सीएचसीडीएस) के घटकों में से एक हैं। 3,18,347 लाभार्थियों को कवर करने वाले 412 बीएलसी को जुलाई, 2015 के बाद से अबतक 557.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, परियोजना की लागत का 212.77 करोड़ रूपया केंद्रीय शेयर के रूप में जारी किया जा चुका है। प्रत्येक समूह को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता कोशल अप-ग्रेडेशन, हाथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद और डिजाइन विकास, कार्यशाला निर्माण, बिजली इकाई, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक रंगाई घर स्थापित करने के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
बुनकर मुद्रा योजना:
बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बुनकर को 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 10,000 रुपये मुनाफा सहायता राशि और क्रेडिट गारंटी भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 443.52 करोड़ रुपये की राशि का 81,615 मुद्रा ऋण प्रदान किया गया है। सितंबर, 2016 में रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा प्लेटफॉर्म को अपनाया गया। मुद्रा प्लेटफॉर्म पर ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया उपयोगकर्ता के अनुकूल है और एटीएम द्वारा रुपे कार्ड का उपयोग करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।
हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल:
वित्तीय सहायता के लिए धन के भुगतान में देरी को कम करने के लिए यह पोर्टल 1 अप्रैल, 2017 से पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से काम कर रही है। बैंक का कहना है कि इस पोर्टल के माध्यम से 25 करोड़ रूपये का निपटारा कर दिया गया है। सहभागी बैंक पोर्टल पर मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क डालते हैं और मार्जिन मनी को सीधे बुनकर के ऋण खाते में स्थानांतरित किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है।
इंडिया हैंडलूम ब्रांड:
हथकरघा उत्पादों की बिक्री से 31.10.2018 तक कुल 582.93 रूपये की कमाई की जा चुकी है। 122 उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत 1185 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग, पर्यावरण पर शून्य प्रभाव और शून्य दोष के साथ प्रामाणिक डिजाइन के लिए किया गया।
बुनकरमित्र:
हथकरघा बुनकरों उत्तर देने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18002089988 शुरू किया गया। बुनकरमित्र हेल्पलाइन के माध्यम से 30.11.2018 तक तकनीकी, कच्चे माल की आपूर्ति, गुणवत्ता नियंत्रण, ऋण सुविधा, बाजार लिंक तक पहुंच जैसे विस्तृत श्रृंखला वाले 22,033 प्रश्नों की जानकारी दी गई। अप्रैल 2017 में स्थापित की गई यह हेल्पलाइन, सप्ताह में 7 दिन हथकरघा बुनकरों को उनके पेशेवर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए देश भर में एकल बिंदु संपर्क प्रदान करती है। टोल-फ्री नंबर के माध्यम से सात भाषाओं में से सेवाएं उपलब्ध हैं: हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया और कन्नड़।
सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):
मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ 7 अगस्त 2017 को ई-कॉमर्स सहित आईटी-सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। प्रत्येक सीएससी को 3,78,400 रूपये की लागत से हैण्डलूम पॉकेट्स, क्लस्टर्स और 28 बुनकर सेवा केंद्रों में खोला गया है। अब तक स्वीकृत 162 सीएससी में से 129 सीएससी कार्यरत हैं।
ई-मार्केटिंग के माध्यम से हथकरघा को बढ़ावा:
हथकरघा उत्पादों के ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, ई-कॉमर्स की 21 इकाइयां ऑनलाइन मार्केटिंग में लगी हुई है। अब तक, कुल 21.25 करोड़ रुपये की बिक्री की जा चुकी है। बुनकरों और उनके परिवारों के आजीविका को सशक्त बनाने के लिए करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मंत्रालय एससी, एसटी, बीपीएल और महिला शिक्षार्थियों को एनआईओएस/ इग्नू के पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत शुल्क की अदायगी करती है।
पावरलूम क्षेत्र
पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए जनवरी 2017 से पूरे देश में 487.07 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ‘पॉवरटैक्स’ नामक एक व्यापक योजना की शुरूआत की गई। नवंबर 2018 तक घटक वार उपलब्धियां निम्नलिखित है:
समतल पावरलूम का यथावत् उन्नतीकरण: 197775 करघों का उन्नयन किया गया और 248.77 करोड़ रूपये जारी किए गए।
सामुहिक कार्यशाला योजना (जीडब्लुएस): इसमें 1034 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 85.64 करोड़ रुपये जारी किए गए।
यार्न (कच्चा धागा) बैंक योजना: 73 यार्न बैंक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 23.263 करोड़ रूपये जारी किए गए।
सामान्य सेवा केंद्र (सीएफसी): 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 3.944 करोड़ रूपये जारी किए गए।
पावरलूम योजनाओं की सुविधा, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार के लिए 15.779 करोड़ रूपये जारी किए गए।
टैक्स वेंचर कैपिटल फंड: 9.34 करोड़ रूपये एसभीसीएल द्वारा अब तक चार कंपनियों को वितरित किया गया है।
पावरलूम सेवा केंद्रों को अनुदान सहायता: 2.99 करोड़ रूपये जारी किए गए।
पावरलूम सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण: 3.39 करोड़ रुपये जारी किए गए।
पावरटैक्स इंडिया के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.ipowertexindia.gov.inhas शुरू की गई है।
दिनांक 1.12.2017 से ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का संचालन शुरू किया गया है।
लाभार्थी मोबाइल ऐप पर वस्तु-स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है।
पावरलूम को चलाता हुआ एक श्रमिक
एकीकृत टेक्सटाईल पार्क योजना (एसआईटीपी)
इस योजना का विस्तार 2017 से 2020 की अवधि तक के लिए किया गया है।
कुल 65 टेक्सटाइल पार्क।
पिछले चार वर्षों 2014-18 में 20 नए टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
इन 20 पार्कों के माध्यम से 6834 करोड़ रूपये तक के निवेश की सुविधा होगी और लगभग 65,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
अब तक कुल 21 पार्कों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 5 पार्क पिछले चार वर्षों (2014-18) में बन चुके हैं।
एकीकृत प्रक्रिया विकास योजना (आईपीडीएस):
इस योजना का विस्तार 2017 से 2020 की अवधि तक के लिए किया गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो कि लगभग 1400 एसएमई इकाइयों को राहत प्रदान कर रही है और कपड़ा प्रौद्योगिकी में 'शून्य प्रभाव' को बढ़ावा दे रही है।
प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्त योजना (टफ्स)
संशोधित टफ्स (एटफ्स) योजना 2016-2022 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया।
पिछली योजनाओं की देनदारियों सहित 17,822 करोड़ रुपये का खर्च
आई-टफ्स के शुरूआत से अंत तक के समाधान के लिए 02.08.2018 को दिशानिर्देशों में संशोधन
स्वीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्त योजना (एटीयुएफएस)
एटीयुएफएस के अंतर्गत 6,468 यूआईडी जारी किए गए।
अनुमानित निवेश- 24,338.75 करोड़ रूपये।
अनुमानित सब्सिडी 1,9595 करोड़ रूपये।
कुल जारी सब्सिडी 8156 करोड़ रूपये।
हस्तकला क्षेत्र
मध्य प्रदेश में बुनकरों को पहचान कार्ड का वितरित
‘पहचान पहल’ के अंतर्गत 22.40 लाख आवेदन प्राप्त हुए और 17.83 लाख पहचान पत्र जारी किए गए। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को योजनाओं के लाभ तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए आधारकार्ड आधारित पहचान पत्र प्रदान करने की योजना की शुरूआत 7 अक्टूबर, 2016 को की गई। 28.5 करोड़ रुपये प्रति लागत वाले नए मेगा क्लस्टर बरेली, लखनऊ और कच्छ में जम्मू और कश्मीर में 20.00 करोड़ रूपये के खर्च के साथ के स्वीकृत किए गए हैं, और काम जारी है।
कपड़ा को पर्यटन के साथ जोड़ने की परियोजना में, ओडिशा में रघुराजपुर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति को पर्यटन स्थलों के रूप में संपूर्ण विकास के लिए चुना गया।
झारखंड, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के 1,58,805 कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए हस्तशिल्प के एकीकृत विकास और संवर्धन के लिए विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
3.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत वाली नए शहरी हाट परियोजना ममल्लापुरम (चेन्नई) और एलुरु (आंध्र प्रदेश) के लिए स्वीकृत की गई.।
पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान आयोजित कार्यक्रम और लाभान्वित कारीगर:
अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना: 435 कार्यक्रमों का आयोजन 58.40 करोड़ रूपये राशि की लागत से किया गया, जिससे 306583 कारीगर लाभान्वित हुए।
डिजाइन और प्रौद्योगिकी का उन्नयन: 756 कार्यक्रमों का आयोजन 53.33 करोड़ रूपये राशि की लागत से किया गया, जिससे 29570 कारीगर लाभान्वित हुए।
विपणन सहायता और सेवाएँ: 787 कार्यक्रमों का आयोजन 87.61 करोड़ रूपये राशि की लागत से किया गया जिससे 58526 कारीगर लाभान्वित हुए।
मानव संसाधन विकास: 2182 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 93.07 करोड़ रुपये राशि की लागत से किया गया, जिससे 46481 कारीगर लाभान्वित हुए।
अनुसंधान और विकास: 702 कार्यक्रमों का आयोजन 23.39 करोड़ रुपये राशि की लागत से किया गया, जिससे 17550 कारीगर लाभान्वित हुए।
कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ: 58.40 करोड़ रुपया मंजूर किया गया, जिससे 478089 कारीगरों को लाभ मिला।
आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहायता: आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए 98.76 करोड़ रुपया मंजूर किया गया।
व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास (मेगा क्लस्टर): 226.65 करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया, जिससे 71915 कारीगरों को लाभ मिला।
हस्तकला सहयोग शिविर: देश भर में 302 स्थानों पर हस्तकला सहयोग शिवियों का आयोजन किया गया, जिसमें 73291 कारीगरों ने भाग लिया। 5155 टूल किटों का वितरण किया गया।
मुद्रा लोन: मुद्रा लोन स्वीकृत किया गया, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 695 विपणन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हस्तशिल्प पुरस्कार: 2014 से लेकर 2016 तक 23 शिल्प गुरुओं और 65 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं (15 महिला कारीगरों सहित) को हस्तशिल्प के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया।
अक्टूबर 2018 में मार्जिन मनी के नए घटक का अनुमोदन किया गया है, जिससे कि अधिकतम 10,000 रूपये तक की स्वीकृत ऋण राशि का मुद्रा लोन 20 प्रतिशत की दर से प्राप्त करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाया जा सके।
हस्तकला का प्रचार:
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2018 तक एसी/ एटी कारीगरों के लिए 24 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे लगभग 1000 एसी/ एटी कारीगर लाभान्वित हुए।
कारीगर हस्तकला सामान बनाते हुए
कालीन बुनाई को बढ़ावा:
कश्मीर में कालीन बुनाई
4 महीने का क्लस्टर प्रशिक्षण का आयोजन पारंपरिक कालीन बुनाई क्षेत्र मे किया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर में।
कारीगरों के एक समूह के लिए 50 लाख की लागत से सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण, जिसमें कच्चे माल का भंडारण के लिए गोदाम, इंटरनेट सुविधाएं, कार्यालय, टॉयलेट और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध।
कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा नेशनल सेंटर फॉर डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट (NCDPD) के सहयोग से इसे लागू कर रहा है।
हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात:
हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात 2014-15 में 20000.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 22916 करोड़ रुपये हो गया।
कालीन का निर्यात 2014-15 में 8441.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 9205.90 करोड़ रूपये हो गया।
हस्तशिल्प क्षेत्र में विदेशी डिजाइनरों को वीजा में छूट
हस्तशिल्प क्षेत्र विदेशी डिजाइनरों को रोजगार वीजा देने के लिए न्यूनतम वेतन की शर्त (16.25 लाख रुपये प्रति वर्ष) में 2 वर्ष की अवधि के लिए यानि 30.06.2020 तक छूट दी गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच) ने विदेशी डिजाइनरों को रोजगार वीजा देने में न्यूनतम वेतन शर्त से छूट प्राप्त करने के केंद्रीय वस्त्र मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। वस्त्र मंत्री द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र में वीजा छूट प्राप्त करने की त्वरित कार्रवाई से निर्यातकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय रुझानों के साथ उत्पादों का विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों को नौकरी देने में मदद मिलेगी।
कपास
कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
कपास किसानों के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष बीज कपास (कपास) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।
फसल सीजन 2018-19 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में पिछले वर्ष की तुलना में 1,130 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) कपास के मूल्य समर्थन के निर्धारण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
सीसीआई एमएसपी संचालन का कार्य करता है जब बाजार में बीज कपास की कीमत एमएसपी दर से नीचे आ जाती है।
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
सीसीआई ने कई प्रगतिशील उपाय किए हैं:
अपनी शाखाओं और कॉर्पोरेट कार्यालयों की सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक जल्द पहुंच बनाने में सीसीआई को सक्षम बनाने के लिए ईआरपी प्रणाली "प्रगति" को अपनाया।
कपास किसानों की पहचान के लिए कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम विकसित किया।
कपास किसानों के लिए एमएसपी का पूरा लाभ प्रदान करने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए उनके खाते में 100 प्रतिशत राशि का सीधा ऑनलाइन भुगतान की पहल।
कपास किसान को कपास के संबंध में नीतिगत पहलों और सीसीआई द्वपा एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने के लिए किसान अनुकूल मोबाइल ऐप "कॉट-एली" विकसित किया।
सीसीआई ने लिंट कॉटन गांठों और कपास बीज की 100 प्रतिशत बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से शुरू किया।
ऑनलाइन स्टॉक प्रबंधन के लिए विकसित गोदाम प्रबंधन प्रणाली।
समय और धन को बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाखा संचालन की निगरानी/ शाखा प्रमुखों के साथ बैठक की शुरूआत की।
100 प्रतिशत कैशलेस लेनदेन को अपनाया।
राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) का पुनरुत्थान:
निवल संपत्ति सकारात्मक होने के कारण, एनटीसी अब एक बीमार कंपनी नहीं रही और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) के परिधि से बाहर आ गई। 31 मार्च 2018 तक इसकी निवल संपत्ति 1,885.87 करोड़ रूपये थी।
ऊन क्षेत्र को बढ़ावा:
कश्मीर का पशमीना शॉल
पशमीना योजना के तहत 4 वर्षों (2014-15 से 2017-18) के लिए कुल 4.47 करोड़ रूपये का अनुदान।
लेह और कारगिल के 340 परिवारों को जानवरों के फाउंडेशन स्टॉक का वितरण।
नस्ल में सुधार के लिए 459 उच्च गुणवत्ता पशमीना हिरन वितरित किए।
दो लाख पश्मीना बकरियों को स्वास्थ्य कवरेज और दवाइयां सालाना और 40,000 बकरियों को पूरक आहार सालाना दिया।
3 प्रजनन फार्मों और 3 आहार बैंकों को सुदृढ़ किया और प्रवासी मार्गों पर 3 चारागाह खेतों का निर्माण किया।
पशमीना की उत्पादकता प्रति बकरी 9.30 प्रतिशत बढ़ी।
लद्दाख क्षेत्र में खानाबदोशों के लिए 775 टेंट और 100 घर उपलब्ध कराए।
पांच सोलरयुक्त सामुदायिक केंद्रों का निर्माण।
जानवरों के "हेल्थ केयर" के लिए "भेड़ और ऊन सुधार योजना" (स्वीस) के माध्यम से 40 लाख भेड़ों को लाभ पहुंचाया।
जूट क्षेत्र
जूट मिल में जूट फाइबर के बंडल
मंत्रालय ने 2014-15 से 2018-19 के बीच पांच वर्षों की अवधि के लिए "स्कीम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द टैक्सटाइल इंडस्ट्री इनक्लुडिंग जूट" की शुरूआत की है, जिसका वित्तीय परिव्यय 149 करोड़ रूपया है। इस योजना के तीन आधारभूत घटक हैं:
घटक- I: कपड़ा और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (वित्तीय परिव्यय 50 करोड़ रुपये)
घटक- II: जूट क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; जूट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रचार-प्रसार गतिविधियों का परिवहन (वित्तीय परिव्यय 80 करोड़ रूपये)
घटक- III: मानदण्ड अध्ययन, ज्ञान प्रसार और आर एंड डी के माध्यम से हरित पहल को बढ़ावा देना (वित्तीय परिव्यय 15 करोड़ रुपये)
वित्तीय सहायता : उपरोक्त 3 घटकों में से किसी भी मामले में, अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए, इस योजना में कुल परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत तक धन देने का प्रावधान है और शेष राशि की व्यवस्था संबंधित परियोजना की कार्यकारी एजेंसी को करनी पड़ेगी। इसी प्रकार, बुनियादी अनुसंधान के लिए इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया जाएगा।
जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंड का विस्तार:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के अंतर्गत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे का विस्तार करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जो निम्नलिखित अनुसार है:
जूट के थैलों में 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी अनिवार्य रूप से पैक किया जाएगा। विविध जूट के थैलों में चीनी को पैक करने के निर्णय से जूट उद्योग में परिवर्तन को गति मिलेगी।
शुरुआत में खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए जूट के थैलों के 10 प्रतिशत मांगपत्रों को उल्टी नीलामी के माध्यम से जीईएम पोर्टल पर रखा जाएगा। यह धीरे-धीरे मूल्य प्रकटीकरण की एक शासन पद्वति में तब्दील हो जाएगा।
इस निर्णय से कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने, जूट क्षेत्र में परिवर्तन लाने और जूट उत्पाद की मांग को बढ़ावा देने और जूट के मांग को बनाए रखने में मदद मिलेगी जो कि जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रोत्साहन का काम करेगा।
जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है जो कि प्रत्येक वर्ष 6,500 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का जूट बैग खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए खरीदता है। यह जूट क्षेत्र के मुख्य मांग को बनाए रखने के लिए और इस क्षेत्र पर निर्भर श्रमिकों और किसानों की आजीविका में सहयोग करने के लिए किया जाता है।
इस निर्णय से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित किसानों और श्रमिकों को लाभ होगा, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के किसानों और श्रमिकों को। लगभग 3.7 लाख श्रमिक और कई लाख किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए जूट क्षेत्र पर निर्भर हैं।
जूट क्षेत्र को सरकार का समर्थन:
कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए मध्यवर्तन के द्वारा, जिसे जूट आईसीएआर कहा जाता है, सरकार एक लाख जूट किसानों को उन्नत कृषि अभ्यासों के प्रसार के लिए सहायता कर रही है जैसे कि लाइन ड्रिल के उपयोग से बुवाई, व्हील होइंग और नेल वीडर्स का उपयोग करके खरपतवार प्रबंधन, गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का वितरण और माइक्रोबियल सहायता प्राप्त रेटिंग। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है और जूट किसानों की आय में प्रति हेक्टेयर 10,000 रूपये की वृद्धि हुई है।
जूट किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) को 2018-19 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है जिससे कि यह एमएसपी का संचालन करने और जूट क्षेत्र में मूल्य स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके।
जूट क्षेत्र में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ गठबंधन किया है और गांधीनगर में एक जूट डिजाइन सेल को खोला गया है। इसके अलावा, जूट जियो टेक्सटाइल्स और एग्रो-टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित और विभागों जैसे सड़क परिवहन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को साथ में लिया गया है।
भारत सरकार ने 5 जनवरी, 2017 से जूट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से आयातित जूट के सामान पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दी है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश में 13 रस्सी मिलों में परिचालन फिर से शुरू हुआ, जिससे 20,000 श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा, निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से भारतीय जूट उद्योग के लिए घरेलू बाजार में 2 लाख मीट्रिक टन जूट के सामान की अतिरिक्त मांग की गुंजाइश बनी है।
जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2016 में, जूट स्मार्ट के नाम से एक ई-सरकार पहल शुरू की गई, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा अस्वीकार किए गए बी-टवील की खरीद करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है। इसके अलावा, एमएसपी और वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत जूट की खरीद के लिए जेसीआई किसानों को 100 प्रतिशत धनराशि का स्थनांतरण ऑनलाइन कर रहा है।
तकनीकी वस्त्र
तकनीकी वस्त्र वह कपड़ा सामग्री और उत्पाद है जो मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें केवल कपड़ों में नहीं, बल्कि कृषि, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, खेल, रक्षा और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी आवेदन प्राप्त होते हैं। एनईआर में भू-तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के लिए 427 करोड़ रुपये के फंड परिव्यय के साथ इसे वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए प्रारंभ किया गया।
105 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ जियोटेक वस्त्र के अंतर्गत 54 परियोजनाएँ सड़क, पहाड़ी ढलान संरक्षण, कुशल जल उपयोग जैसी चीजों की गुणवत्ता के लिए बुनियादी ढाँचे प्रदान करते हैं।
तकनीकी वस्त्रों पर प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 2012-13 से लेकर 2016-17 तक 208 करोड़ के परिव्यय के साथ, उत्कृष्टता के लिए आठ केंद्रों और 11 फोकस ऊष्मायन केंद्रों की स्वीकृति, 10 कृषि-डेमो केंद्रों की स्थापना और 6 राज्यों में 200 एग्रो किट वितरित किए गए।
इस योजना के अंतर्गत, कृषि वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3841 किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद 44 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना और कृषि किसानों के बीच 840 एग्रोटेक्स्टाइल किट का वितरण किया गया।
वस्त्र उद्योग में अनुसंधान और विकास की योजना के अंतर्गत 118 परियोजनाएं हैं जिसमें जूट भी शामिल है। परियोजना की कुल लागत 11,042.86 लाख रूपये हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा विकास और बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़ों के उत्पाद के लिए 7,851.86 लाख की सहायता शामिल है।
टेक्नोटेक्स, तकनीकी वस्त्रों पर भारत का प्रमुख शो, का आयोजन 2014, 2015, 2016 और 2017 में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए फिक्की के सहयोग से किया गया।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वस्त्र प्रमोशन योजना (एनईआरटीपीएस)
यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करती है। इस योजना का परिव्यय 2017-18 से 2019-20 के लिए 500 करोड़ रूपया है।
नागालैंड में शॉल बुनती हुई महिला
नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत, 32 सेरीकल्चर योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्यों में शहतूत, एरी और मुगा क्षेत्रों को कवर करते हुए इंटीग्रेटेड सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईएसडीपी) और इंटेंसिव बिवोल्टाइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईबीएसडीपी) को लागू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य वृक्षारोपण विकास से लेकर उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन के साथ कपड़ों के उत्पादन तक सभी क्षेत्रों में सेरीकल्चर का एकीकृत विकास करना है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट)
वस्त्र मंत्री से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले एनआईएफटी के छात्र
इंडियासाइज नामक एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) द्वारा भारतीय जनसंख्या के लिए शारीरिक माप के आधार पर रेडी-टू-वियर उद्योग के लिए एक व्यापक आकार चार्ट को विकसित करने के लिए किया जाएगा। यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है जहां पर 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु वाले लोगों के एक नमूना जनसंख्या का मानवशास्त्रीय डाटा एकत्र किया जाएगा जिससे कि माप का एक डेटाबेस तैयार किया जा सके, जिसका परिणाम एक मानकीकृत आकार चार्ट होगा जो कि भारतीय आबादी का प्रतिनिधि है और इसे परिधान उद्योग द्वारा भी अपनाया जा सकता है। यह सर्वेक्षण पैन देश में 3 डी तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से पूरे शरीर को स्कैन करके सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक शरीर माप लेने और एकत्रित डेटा का विश्लेषण करने का एक गैर-संपर्क तरीका है।
इस परियोजना में देश के 6 क्षेत्रों के 6 शहरों में 25,000 पुरुष और महिला भारतीयों की माप की जाएगी: कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नई दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य भारत), बेंगलुरु (दक्षिण) और शिलांग (उत्तर पूर्व)। 3 डी संपूर्ण बॉडी स्कैनर का उपयोग करके, कंप्यूटर एक स्कैन से सैकड़ों माप निकाल लेंगे। इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनाया गया डेटा गोपनीय और सुरक्षित होगा। परियोजना की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से लगभग दो वर्ष की होगी।
मानकीकृत आकार चार्ट के अभाव में अच्छे प्रकार की फिटिंग वाली वस्त्र को प्रदान करना घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, जिसका 2021 तक 123 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है और जो परिधान आयात में 5 वां स्थान रखता है।
दुकानदारों का एक बड़ा वर्ग उन कपड़ों को खोजने में कठिनाईयों का सामना करता है जो लोगों के शरीर के माप के अनुसार पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इसका कारण देश भर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के बीच मानवशास्त्रीय अंतर है। अब तक 14 देशों ने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय माप सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं।
भारतीय परिधान उद्योग उस आकार चार्ट का उपयोग करता है जो कि अन्य देशों के आकार चार्टों का संस्करण हैं, इसलिए कपड़ों का रिटर्न 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक है और यह ई-कॉमर्स के वृद्धि के साथ बढ़ रहा है और रिटर्न का मुख्य कारण परिधान की खराब फिटिंग है।
इस अध्ययन की प्राप्ति से विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वचालित, अंतरिक्ष, फिटनेस और खेल, कला और कंप्यूटर गेमिंग प्रभावित होंगे जहां इस डेटा के माध्यम से अंतर्दृष्टि एर्गोनोमिक रूप से डिज़ाइन किए गए उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है जो कि भारतीय आबादी के लिए अनुकूल हैं।
फैशन टेक्नोलॉजी में क्षमता निर्माण:
निफ्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संस्कृति को फिर से खोजने के विषय पर आधारित: ट्रांसफॉर्मिंग फैशन पर आधारित निफ्ट का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 31 जनवरी से 2 फरवरी 2018 तक आयोजित किया गया जो कि उसके तीस साल की यात्रा में एक मील के पत्थर था।
इस सम्मेलन ने फैशन, संस्कृति, वस्त्र, शिल्प और स्थिरता पर वैश्विक आख्यानों के लिए एक बहुविषयक मंच प्रदान किया।
श्रीनगर, (जम्मू और कश्मीर) में 325.36 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत से एक निफ्ट परिसर पर खोला गया। पंचकूला में एक निफ्ट कैंपस के नींव का पत्थर रखा गया। विभिन्न परिसरों में संस्थान के बुनियादी ढांचे जैसे शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल और छात्र केंद्रों को संवर्धित किए जा रहे हैं।
निफ्ट ने नवोदित फैशन पेशेवरों के साथ हथकरघा समूहों को जोड़ने के सहजीवी पहल के लिए “क्लस्टर पहल” के लिए डीसी (हस्तशिल्प) और डीसी (हैंडलूम) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।
पारंपरिक डिजाइनों को पुनर्जीवित करने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए निफ्ट के विस्तार केंद्र की वाराणसी में स्थापना।
उस्ताद (पैतृक कला/ शिल्प में विकास के लिए कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से शुरू किए गए योजना में 25 हस्तकला और हथकरघा समूहों को शामिल करेगा।
जोधपुर मेगा क्लस्टर (हैंडक्राफ्ट) के लिए व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर योजना के अंतर्गत उत्पाद डिजाइन विकास और नवाचार केंद्र को स्थापित करना।
डोनर मंत्रालय के लिए फैशन डिजाइन डेवलपमेंट (सीपीएफडीडी), फैशन डिजाइन एंड मैनेजमेंट (सीपीएफडीएम), सूचना प्रौद्योगिकी में फैशन प्रौद्योगिकी (सीपीएआईटी) और निटवेअर डिजाइन और विनिर्माण (सीपीकेडीएम) के लिए चार वर्षीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम की शुरूआत।
डाक कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, सीआईटी और सीटीएस के कर्मचारियों के लिए यूनफॉर्म का डिजाइन।
निर्यात संवर्धन संस्थान
भारत से ऊनी, रेशम और सेल्यूलोज फाइबर सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत 1 नवंबर 2017 से परिधान में 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि, 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की वृद्धि मेकअप, हथकरधा और हस्तशिल्प मे की है। इसके अलावा, सरकार ने 2 नवंबर, 2018 से टेक्सटाइल क्षेत्र में प्री-पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट के लिए ब्याज समानता दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
रेशम क्षेत्र के लिए, सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारतीय रेशम के आर एंड डी और ब्रांड छवि को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समागम योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरूआत से लेकर कपड़ा उत्पादन के स्तर तक लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है।
वस्त्र, परिधान और मेकअप के लिए पैकेज
विशेष पैकेज
पैकेज का डिज़ाइन एक करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए (31 बिलियन अमरीकी डालर) और 3 साल में 80, 000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए किया गया। आज की तारीख में इसने अबतक 15.68 लाख अतिरिक्त रोजगार की संभावनाएँ पैदा की है, साथ ही अतिरिक्त निर्यात 5,728 करोड़ और 25,345 करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश भी पैदा किया है।
निर्यात को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर को पैदा करने के उद्देश्य से जून और दिसंबर 2016 में 6000 करोड़ के एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई।
प्रधानमंत्री जनप्रतिनि परिधान रोजगार प्रोतसाहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत परिधान और बने-बनाए परिधान के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान के लिए सरकार द्वारा संपूर्ण 12 प्रतिशत का योगदान।
काम के घंटे, वेतन, भत्ते और अन्य वैधानिक देयताओं के संदर्भ में स्थायी काम करने वाले के साथ निश्चित क्षेत्र के कामगार बनाने वाले परिधान क्षेत्र के लिए निश्चित शब्द रोजगार।
परिधान क्षेत्र के लिए निश्चित रोजगार के लिए स्थायी काम करने वालों की तरह घंटे, वेतन, भत्ते और अन्य वैधानिक बकाया का प्रावधान किया गया।
परिधान और बने-बनाए क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत उन्मुख पूंजी निवेश की सब्सिडी में 10 प्रतिशत की वृद्धि।
15 नवंबर, 2018 को निर्यातकों को 4,853.6 करोड़ रूपये रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज जारी की गई। रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज योजना परिधान और बने-बनाए चीजों के लिए विशेष पैकेज के रूप में बनाई गई।
स्वदेशी उत्पादन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 501 कपड़ा उत्पादों पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति:
इसमें बाजारों का विविधीकरण, मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति और सहयोगी निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
विविध बाजार: वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, ब्राजील, चिली, कोलंबिया और पेरू के 12 बाजारों की पहचान की गई है।
मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति: बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ावा दें: फैब्रिक-फ़ॉरवर्ड पॉलिसी
सहयोगात्मक निर्यात को बढ़ावा:
परिधान और अनुबंधित वस्त्र
वस्त्र पार्कों में निवेश आकर्षित करना
जी2जी पहल के तहत पारंपरिक कपड़ों का निर्यात
विविध उत्पाद:
अनुबंधित वस्त्रों की मांग के लिए भारतीय वस्त्रों को एकीकृत करना
जूट बैग का लैटिन अमेरिकी देश के खुदरा विक्रेताओं में आपूर्ति
लैटिन देशों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण
राष्ट्रीय कपड़ा मिशन का गुणवत्ता और अनुपालन के लिए शुभआरंभ
गुणवत्ता और अनुपालन तंत्र को मजबूत करना
गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 31.3.2020 तक 100 करोड़ रूपये।
वेयरहाउस सह प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना: चीन (शंघाई), रूस (मास्को), एलएसी
(कोलंबिया और पेरू के लिए एक पनामा में और एक चिली में ) और सऊदी अरब में।
ई-कॉमर्स प्रदाता के माध्यम से सीमा पार निर्यात को बढ़ावा देना।
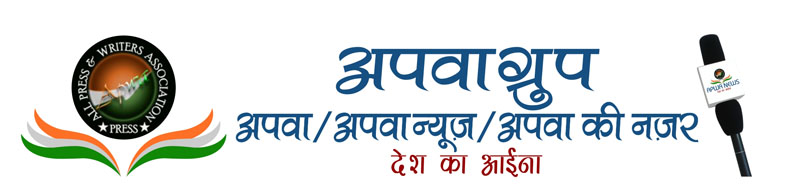


Comments